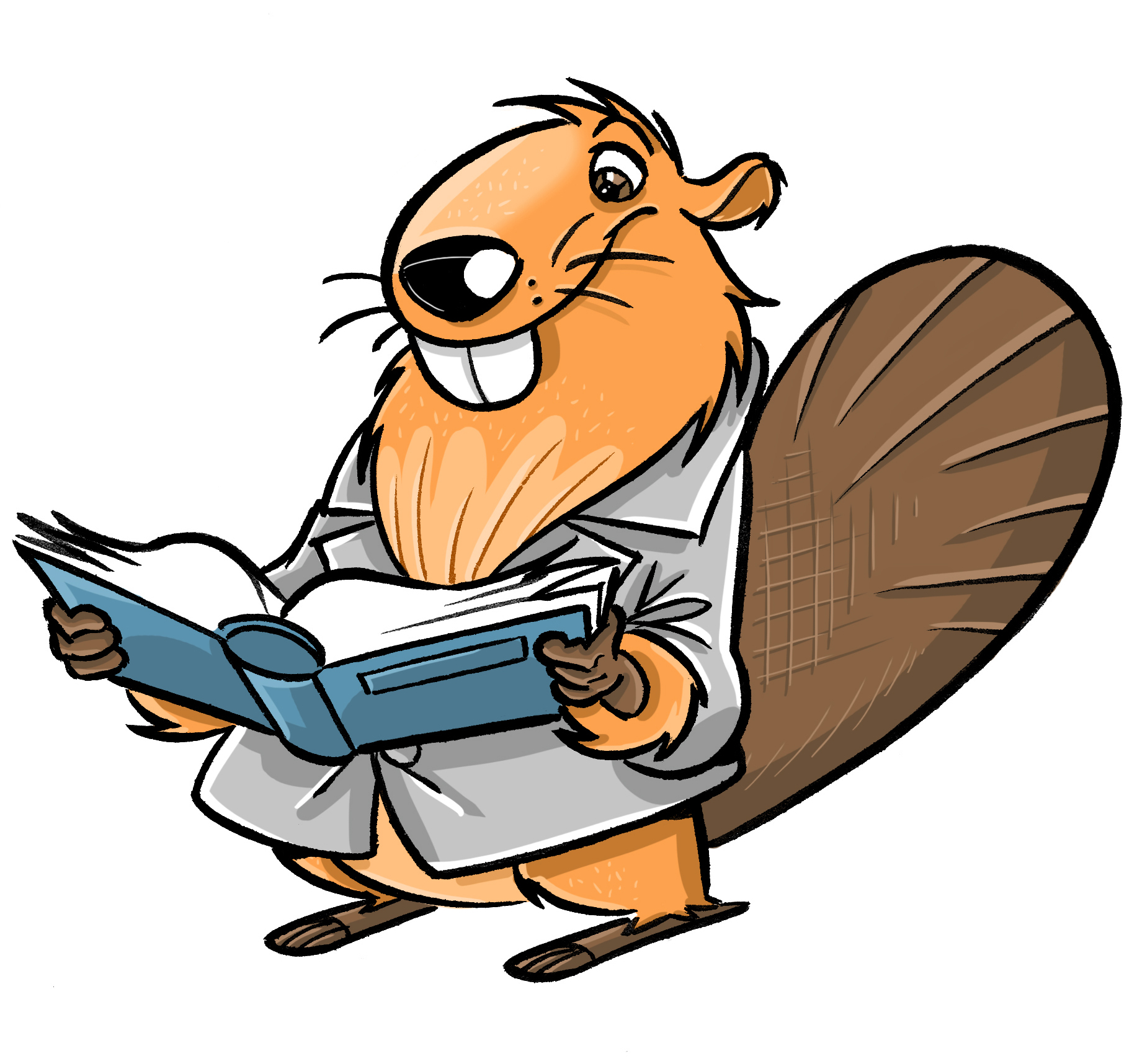1.1 а•Яа§є а§Ха•На•Яа§Њ а§єа•Иа•§
1.1 а•Яа§є а§Ха•На•Яа§Њ а§єа•Иа•§
а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Па§Х а§Ж৮а•Б৵а§В৴ড়а§Х а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•Иа•§ а§За§Є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•З а§Ѓа§∞а•Аа§Ьа•Ла§В а§Ха•Л ১а•Н৵а§Ъа§Њ а§Ѓа•За§В а§≤а§Ња§≤ а§Ъа§Х১а•Н১а•З, а§Ч৆ড়ৃৌ а§Фа§∞ а§Жа§Ба§Ца•Ла§В а§Ха•А ৴ড়а§Хৌৃ১ а§єа•Л১а•А а§єа•Иа•§ а§Е৮а•На§ѓ а§Еа§Ва§Ч а§≠а•А ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ড়১ а§єа•Л১а•З а§єа•И, ১৕ৌ а§∞а•Ба§Х а§∞а•Ба§Х а§Ха§∞ а§ђа•Ба§Ца§Ња§∞ а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§За§Є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•З а§Ж৮а•Б৵а§В৴ড়а§Х а§∞а•В৙ а§Ха•Л а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ ৮ৌু ৶ড়ৃৌ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•И а§≤а•За§Хড়৮ а§Єа•Н৙а•Ла§∞а•З৶ড়а§Х а§∞а•В৙ а§≠а•А а§єа•Л а§Єа§Х১а•З а§єа•И а§Ьа•Л а§Ха•А а§Ыа•Ла§Яа•А а§Йа§Ѓа•На§∞ а§Ѓа•За§В а§єа•Л১а•З а§єа•Иа•§
 1.2 а§ѓа§є а§Хড়১৮ৌ а§Жа§Ѓ а§єа•И ?
1.2 а§ѓа§є а§Хড়১৮ৌ а§Жа§Ѓ а§єа•И ?
а§За§Є а§∞а•Ла§Ч а§Ха•А а§Ж৵а•Г১а•Н১ড় а§Еа§Ьа•На§Юৌ১ а§єа•Иа•§ а§ѓа§є а§Па§Х а§ђа§єа•Б১ ৶а•Ба§∞а•На§≤а§≠ а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•И а§Ьа•Л а§Еа§Іа§ња§Х১а§∞ а•Ђ ৵а§∞а•На§Ј а§Єа•З а§Ха§Ѓ а§Йа§Ѓа•На§∞ а§Ха•З а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•Л ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ড়১ а§Ха§∞১а•А а§єа•И, ১৕ৌ ৃ৶ড় а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ ৮ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Ња§П ১а•Л а§ђа•Э а§Єа§Х১а•А а§єа•Иа•§ а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Єа•З а§Ьа•Ба•Ьа•З а§єа•Ба§П а§Ьа•А৮ а§Ха•А а§Ца•Ла§Ь а§Ха•З ৐ৌ৶ ৮ড়৶ৌ৮ а§Еа§Іа§ња§Х а§ђа§Ња§∞ а§Єа§Ва§≠৵ а§єа•Б৵ৌ а§єа•И, ১৕ৌ а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•Л а§Ча§єа§∞а§Ња§И а§Фа§∞ ৙а•На§∞а§Ња§Ха•Г১ড়а§Х а§Ха•Ла§∞а•На§Є а§Ха§Њ а§ђа•З৺১а§∞ а§Е৮а•Бুৌ৮ а§≤а§Ча§Ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§
 1.3 а§За§Є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•З а§Ха§Ња§∞а§£ а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И ?
1.3 а§За§Є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•З а§Ха§Ња§∞а§£ а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И ?
а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Па§Х а§Ж৮а•Б৵а§В৴ড়а§Х а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•Иа•§ а§За§Єа§Ха•З а§Ьа•А৮ а§Ха•Л NOD2 (৪ুৌ৮ৌа§∞а•Н৕а§Х CARD 15) а§Х৺১а•З а§єа•И, а§Ьа•Л а§Па§Х ৙а•На§∞১ড়а§∞а§Ха•На§Ја§Њ а§Фа§∞ ৙а•На§∞১ড়а§Ха•На§∞а§ња§ѓа§Њ а§Ха•Л ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ড়১ а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•З ৙а•На§∞а•Ла§Яа•А৮ а§Ха•Л а§Ха•Ла§° а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ а§За§Є а§Ьа•А৮ а§Ха•З а§Й১а•Н৙а§∞ড়৵а§∞а•Н১৮ (а§Ьа•Иа§Єа•З а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ѓа•За§В) а§Ха•А ৵а§Ьа§є а§Єа•З ৙а•На§∞а•Ла§Яа•А৮ ৆а•Аа§Х ৥а§Ва§Ч а§Єа•З а§Ха§Ња§Ѓ ৮৺а•Аа§В а§Ха§∞১ৌ а§єа•И а§Ьа§ња§Єа§Єа•З а§З৮ а§∞а•Ла§Ча§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•З ৵ড়а§≠ড়৮а•Н৮ а§К১а§Ха•Ла§В а§Фа§∞ а§Еа§Ва§Ча•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Ча•На§∞а•З৮а•На§ѓа•Ба§≤а•Ла§Ѓа§Њ ১৕ৌ а§≤а§Ѓа•На§ђа•З а§Єа§Ѓа§ѓ ১а§Х а§Єа•Ва§Ь৮ а§∞৺১а•А а§єа•Иа•§ а§Єа•Ва§Ь৮ ৙а•И৶ৌ а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•А а§Ха•Л৴ড়а§Ха§Ња§Уа§В а§Ха•З а§≤а§Ѓа•На§ђа•З а§Єа§Ѓа§ѓ ১а§Х а§Па§Х ৪ৌ৕ а§Єа§Ѓа•Ва§є а§Ѓа•За§В а§∞৺৮а•З а§Єа•З а§Ча•На§∞а•З৮а•На§ѓа•Ба§≤а•Ла§Ѓа§Њ ৐৮১а•З а§єа•И а§Ьа•Л а§Ха§њ ৴а§∞а•Аа§∞ а§Ха•З ৵ড়а§≠ড়৮а•Н৮ а§Еа§Ва§Ча•Ла§В а§Фа§∞ а§К১а§Ха•Ла§В а§Ха•А ৪ৌুৌ৮а•На§ѓ а§Єа§Ва§∞а§Ъ৮ৌ ১৕ৌ а§Ха§Ња§Ѓа§Ха§Ња§Ь а§Ха•Л ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ড়১ а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§
 1.4 а§Ха•На§ѓа§Њ а§ѓа§є а§Ж৮а•Б৵а§В৴ড়а§Х а§єа•И ?
1.4 а§Ха•На§ѓа§Њ а§ѓа§є а§Ж৮а•Б৵а§В৴ড়а§Х а§єа•И ?
а§ѓа§є а§Ж৮а•Б৵а§В৴ড়а§Х а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•Л১а•А а§єа•Иа•§ (а§ѓа§є а§≤а§ња§Ва§Ч а§Єа§В৐৲ড়১ ৮৺а•Аа§В а§єа•И ১৕ৌ ুৌ১ৌ৙ড়১ৌ а§Ѓа•За§В а§Єа•З а§Ха§Ѓ а§Єа•З а§Ха§Ѓ а§Па§Х а§Ѓа•За§В а§За§Єа§Ха•З а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§єа•Л৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§П) а§За§Єа§Ха§Њ а§Еа§∞а•Н৕ а§єа•И а§Ха§њ а§∞а•Ла§Ча•А а§Ха•З ুৌ১ৌ ৙ড়১ৌ а§Ѓа•За§В а§Па§Х а•Ща§∞а§Ња§ђ а§Ьа•А৮ а§єа•Л৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§ Sporadic а§Ђа•Йа§∞а•На§Ѓ а§Ѓа•За§В а§Й১а•Н৙а§∞ড়৵а§∞а•Н১৮ (а§Ѓа•На§ѓа•Ва§Яа•З৴৮) а§Єа•Н৵ৃа§В а§∞а•Ла§Ча•А а§Ѓа•За§В а§єа•Л১ৌ а§єа•И ১৕ৌ ুৌ১ৌ৙ড়১ৌ а§Єа•Н৵৪а•Н৕ а§єа•Л১а•З а§єа•Иа•§ ৃ৶ড় а§∞а•Ла§Ча•А а§Ѓа•За§В а§Ьа•А৮ а§єа•Л১ৌ а§єа•И ১а•Л ৵৺ а§За§Є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Єа•З ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ড়১ а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§ ৃ৶ড় ুৌ১ৌ৙ড়১ৌ а§Ѓа•За§В а§Єа•З а§Ха§ња§Єа•А а§Па§Х а§Ха•Л а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§єа•И ১а•Л а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ѓа•За§В а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•А а§Єа§Ва§≠ৌ৵৮ৌ а•Ђа•¶% а§єа•Л১а•А а§єа•Иа•§
 1.5 а§Ѓа•За§∞а•З а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ѓа•За§В а§ѓа§є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•На§ѓа•Ла§В а§єа•И ? а§Ха•На§ѓа§Њ а§За§Єа•З а§∞а•Ла§Ха§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И?
1.5 а§Ѓа•За§∞а•З а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ѓа•За§В а§ѓа§є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•На§ѓа•Ла§В а§єа•И ? а§Ха•На§ѓа§Њ а§За§Єа•З а§∞а•Ла§Ха§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И?
а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ѓа•За§В а§За§Є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха§Њ а§Ьа•А৮ а§єа•И а§Ьа•Л а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ха§Њ а§Ха§Ња§∞а§£ а§єа•Иа•§ а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•Л а§∞а•Ла§Х ৮৺а•Аа§В а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§≤а•За§Хড়৮ а§За§Єа§Ха•З а§≤а§Ха•На§Ја§£а•Ла§В а§Ха§Њ а§За§≤а§Ња§Ь а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§
 1.6 а§Ха•На§ѓа§Њ а§ѓа§є а§Ыа•В১ а§Ха•А а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•И?
1.6 а§Ха•На§ѓа§Њ а§ѓа§є а§Ыа•В১ а§Ха•А а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•И?
৮৺а•Аа§Ва•§
 1.7 а§Ѓа•Ба§Ца•На§ѓ а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И?
1.7 а§Ѓа•Ба§Ца•На§ѓ а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И?
а§Ѓа•Ба§Ца•На§ѓ а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§Жа§∞а•Н৕а§∞а§Ња§За§Яа§ња§Є (а§Ч৆ড়ৃৌ), а§°а§∞а•На§Ѓа•За§Яа§Ња§За§Яа§ња§Є, а§ѓа•В৵ৌа§За§Яа§ња§Є ১а•Н৵а§Ъа§Њ а§П৵а§В а§Жа§Ба§Ца•Ла§В а§Ха•А ১а§Ха§≤а•Аа§Ђ а§єа•Иа•§ ৴а•Ба§∞а•Ба§Ж১а•А а§≤а§Ха•На§Ја§£, а§Па§Х ৵ড়৴ড়ৣа•На§Я ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•З ৶ৌ৮а•З а§єа•И а§Ьа•Л а§Ха•А а§Ыа•Ла§Яа•З а§Ча•Ла§≤ а§єа§≤а§Ха•З а§Ча•Ба§≤а§Ња§ђа•А а§∞а§Ва§Ч а§Єа•З а§Ча§єа§∞а•З а§Е৕৵ৌ ১а•А৵а•На§∞ а§≤а§Ња§≤৙৮ а§Ха•А ১а§∞а§є а§єа•Л а§Єа§Х১а•З а§єа•И а§Ха§≠а•А - а§Ха§≠а•А ৶ৌ৮а•З а§Ха§Ѓ а§ѓа§Њ а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ а§єа•Л а§Єа§Х১а•З а§єа•Иа•§ а§Ч৆ড়ৃৌ а§Єа§ђа§Єа•З а§Жа§Ѓ а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§єа•И, а§Ьа•Л ৙৺а§≤а•З ৶৴а§Х а§Ѓа•За§В ৴а•Ба§∞а•В а§єа•Л а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§ ৴а•Ба§∞а•Ба§Ж১ а§Ѓа•За§В а§Ьа•Ла•Ьа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Єа•Ва§Ь৮ а§Ж১а•А а§єа•И ৙а§∞ а§Ъа§≤৮а•З а§Ѓа•За§В ১а§Ха§≤а•Аа§Ђ ৮৺а•Аа§В а§єа•Л১а•Аа•§ а§Іа•Аа§∞а•З а§Іа•Аа§∞а•З а§Ъа§≤৮а•З а§Ђа§ња§∞৮а•З а§Ѓа•За§В ১а§Ха§≤а•Аа§Ђ ১৕ৌ ৵ড়а§Ха•Г১ড় а§ђа•Э১а•З а§Ьৌ১а•З а§єа•Иа•§ а§ѓа•В৵ৌа§За§Яа§ња§Є (а§Жа§За§∞а§ња§Є а§Ха•А а§Єа•Ва§Ь৮), а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ а§Ц১а§∞৮ৌа§Х а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•И а§Ха•На§ѓа•Ла§Ва§Ха§њ а§ѓа§є а§Еа§Ха•На§Єа§∞ а§Ьа§Яа§ња§≤১ৌа§Па§В ৶а§∞а•Н৴ৌ১ৌ а§єа•И (а§Ьа•Иа§Єа•З а§Ѓа•Л১ড়ৃৌ৐ড়а§В৶, а§Жа§Ца•Ла§В а§Ха•З а§Еа§В৶а§∞ ৶৐ৌ৵ а§ђа•Э৮ৌ а§Ж৶а•А ) ১৕ৌ ৃ৶ড় а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ ৮ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Ња§П ১а•Л ৶а•Га§Ја•На§Яа•А а§Ха§Ѓ а§єа•Л а§Єа§Х১а•А а§єа•Иа•§
а§За§Єа§Ха•З ৪ৌ৕ а§єа•А а§Ча•На§∞а•З৮а•На§ѓа•Ба§≤а•Ла§Ѓа§Њ а§≠а•А ৶а•Ва§Єа§∞а•З а§Еа§Ва§Ча•Л а§Ха•Л ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ড়১ а§Ха§∞১ৌ а§єа•И а§Фа§∞ а§Е৮а•На§ѓ а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§Ьа•Иа§Єа•З а§Ђа•За§Ђа•Ьа•З ১৕ৌ а§Ча•Ба§∞а•Н৶а•З а§Ха•А а§Ца§∞а§Ња§ђа•А а§∞а§Ха•Н১ а§Ъৌ৙ а§Ха§Њ а§ђа•Э৮ৌ ১৕ৌ а§ђа§Ња§∞ а§ђа§Ња§∞ а§ђа•Ба§Ца§Ња§∞ а§Ха§Њ а§Ха§Ња§∞а§£ а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§
 1.8 а§Ха•На§ѓа§Њ а§ѓа§є а§∞а•Ла§Ч ৙а•На§∞১а•На§ѓа•За§Х а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ѓа•За§В ৪ুৌ৮ а§єа•Л১ৌ а§єа•И?
1.8 а§Ха•На§ѓа§Њ а§ѓа§є а§∞а•Ла§Ч ৙а•На§∞১а•На§ѓа•За§Х а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ѓа•За§В ৪ুৌ৮ а§єа•Л১ৌ а§єа•И?
а§ѓа§є а§єа§∞ а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ѓа•За§В ৪ুৌ৮ ৮৺а•Аа§В а§єа•Ла§§а§Ња•§ а§ђа•Э১а•А а§Йа§Ѓа•На§∞ а§Ха•З ৪ৌ৕ а§За§Єа§Ха•З а§≤а§Ха•На§Ја§£а•Ла§В а§Ха•З ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Фа§∞ а§Ча§Ва§≠а•Аа§∞১ৌ ৐৶а§≤ а§Єа§Х১а•А а§єа•Иа•§ ৃ৶ড় а§Єа§Ѓа§ѓ ৙а§∞ а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ ৮ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Ња§П ১а•Л а§∞а•Ла§Ч а§Фа§∞ а§За§Єа§Ха•З а§≤а§Ха•На§Ја§£а•Ла§В а§Ѓа•За§В ৵а•Г৶а•На§Іа§њ а§єа•Л а§Єа§Х১а•А а§єа•Иа•§
 2.1 а§За§Єа§Ха§Њ ৮ড়৶ৌ৮ а§Ха•Иа§Єа•З а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•И?
2.1 а§За§Єа§Ха§Њ ৮ড়৶ৌ৮ а§Ха•Иа§Єа•З а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•И?
а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ха§Њ ৮ড়৶ৌ৮ ৪ৌুৌ৮а•Нৃ১а§Г ৮ড়ুа•Н৮ а§∞а•В৙ а§Єа•З а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•Иа•§
а§Ъа§ња§Хড়১а•На§Єа§Ха•Аа§ѓ ৴а§Ва§Ха§Њ : а§Ьа§ђ а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•Л а§Єа§Ва§ѓа•Ба§Ха•Н১ а§∞а•В৙ а§Єа•З (а§Ьа•Ла•Ь, ১а•Н৵а§Ъа§Њ а§П৵а§В а§Жа§Ба§Ц ) а§Єа§≠а•А а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§Па§Х ৪ৌ৕ а§Ж১а•За§В а§єа•И ১а•Л а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ ৆а•Аа§Х ১а§∞а§є а§Єа•З ৙ৌа§∞ড়৵ৌа§∞а§ња§Х а§Ьৌ৮а§Ха§Ња§∞а•А а§≤а•З৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§П а§Ха•На§ѓа•Ла§Ва§Ха§њ а§ѓа§є а§ђа§єа•Б১ ৶а•Ба§∞а•На§≤а§≠ а§∞а•Ла§Ч а§єа•И ১৕ৌ а§Са§Яа•Ла§Єа•Ла§Ѓа§≤ а§°а•Лুড়৮а•За§Ва§Я а§∞а•В৙ а§Ѓа•За§В ৵а§В৴ৌ৮а•Ба§Ч১ а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§
а§Ча•На§∞а•З৮а•На§ѓа•Ба§≤а•Ла§Ѓа§Њ а§Ха§Њ ৙а•На§∞৶а§∞а•Н৴৮ : а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ха•З ৮ড়৶ৌ৮ а§Ха•З а§≤а§ња§П ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ড়১ а§Еа§Ва§Ча•Ла§В а§Ѓа•За§В а§Па§Х ৵ড়৴ড়ৣа•На§Я а§Ча•На§∞а•З৮а•На§ѓа•Ба§≤а•Ла§Ѓа§Њ а§Ха•А а§Й৙৪а•Н৕ড়১ড় а§Ж৵৴а•На§ѓа§Х а§єа•Л১а•А а§єа•Иа•§ ১а•Н৵а§Ъа§Њ а§Е৕৵ৌ а§Єа•Ва§Ьа•З а§єа•Ба§П а§Ьа•Ла•Ьа•Л а§Ха•А а§ђа§Ња§ѓа•Л৙а•На§Єа•А а§Ѓа•За§В а§Ча•На§∞а•З৮а•На§ѓа•Ба§≤а•Ла§Ѓа§Њ ৶а•За§Ца•З а§Ьа§Њ а§Єа§Х১а•З а§єа•Иа•§ а§Ча•На§∞а•З৮а•На§ѓа•Ба§≤а•Ла§Ѓа•З а§Ха•З а§Е৮а•На§ѓ а§Ха§Ња§∞а§£ (а§Ьа•Иа§Єа•З а§Яа•А. а§ђа•А., ৵ৌ৪а§Ха•На§ѓа•Ба§≤а§Ња§За§Яа§ња§Є , а§За§Ѓа•На§ѓа•В৮ а§°а•Зীড়৴ড়а§П৮а•На§Єа•А ) а§Ха•Л а§°а•Йа§Ха•На§Яа§∞а•А а§Ьа§Ња§Ба§Ъ, а§Ца•В৮ а§Ха•А а§Ьа§Ња§Ба§Ъ ১৕ৌ а§За§Ѓа•За§Ьа§ња§Ва§Ч а§Ха•З ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ а§Еа§≤а§Ч а§Ха§∞ а§≤а•З৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§
а§Ьа•З৮ড়а§Яа§ња§Х ৵ড়ৣа•На§≤а•За§Ја§£ : ৙ড়а§Ыа§≤а•З а§Ха•Ба§Ы ৵а§∞а•На§Ја•Ла§В а§Ѓа•За§В, а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§≤а§ња§П а§Ьа§ња§Ѓа•На§Ѓа•З৶ৌа§∞ а§Ьа•З৮а•За§Яа§ња§Х а§Ѓа•На§ѓа•Ба§Яа•З৴৮ ৵ড়ৣа•На§≤а•За§Ја§£ а§Єа§Ва§≠৵ а§єа•Л а§Ча§ѓа§Њ а§єа•Иа•§
 2.2 ৙а§∞а§ња§Ха•На§Ја§£ а§Ха§Њ а§Ха•На§ѓа§Њ ু৺১а•Н৵ а§єа•И ?
2.2 ৙а§∞а§ња§Ха•На§Ја§£ а§Ха§Њ а§Ха•На§ѓа§Њ ু৺১а•Н৵ а§єа•И ?
১а•Н৵а§Ъа•Аа§ѓ а§ђа§Ња§ѓа•Л৙а•На§Єа•А: а§За§Є ৙а§∞а§ња§Ха•На§Ја§£ а§Ѓа•За§В ১а•Н৵а§Ъа§Њ а§Ха•З а§Па§Х а§Ыа•Ла§Яа•З а§Яа•Ба§Ха•Ьа•З а§Ха•Л ৮ড়а§Ха§Ња§≤а§Ха§∞ а§Ьа§Ња§Ба§Ъ а§Ха•А а§Ьৌ১а•А а§єа•И а§Фа§∞ а§ѓа§є а§ђа§єа•Б১ а§Ж৪ৌ৮ а§єа•Иа•§ ৃ৶ড় ১а•Н৵а§Ъа§Њ а§Ха•А а§ђа§Ња§ѓа•Л৙а•На§Єа•А а§Ѓа•За§В а§Ча•На§∞а•З৮а•На§ѓа•Ба§≤а•Ла§Ѓа§Њ ৙ৌৃৌ а§Ьа§Ња§П ১а•Л а§ѓа§є а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ха•А ৙а•Ба§Ја•На§Яа§њ а§Ха§∞১ৌ а§єа•И ১৕ৌ а§Е৮а•На§ѓ а§Єа§≠а•А а§Ча•На§∞а•З৮а•Ба§≤а•Ла§Ѓа§Њ а§Ха•З а§Ха§Ња§∞а§£а•Ла§В а§Ха•Л а§Еа§≤а§Ч а§Ха§∞১ৌ а§єа•И а•§
а§∞а§Ха•Н১ ৙а§∞а•Аа§Ха•На§Ја§£: а§∞а§Ха•Н১ ৙а§∞а•Аа§Ха•На§Ја§£ а§Ча•На§∞а•З৮а•На§ѓа•Ба§≤а•Ла§Ѓа•З а§Ха•З а§Е৮а•На§ѓ а§Ха§Ња§∞а§£а•Ла§В (а§Ьа•Иа§Єа•З а§Ха•На§∞а•Л৮а•На§Є а§Е৕৵ৌ а§За§Ѓа•На§ѓа•В৮ а§°а•Зীড়৴ড়ৃа•За§Ва§Єа•А ) а§Ха•Л а§Еа§≤а§Ч а§Ха§∞১ৌ а§єа•Иа•§ а§ѓа§є а§Єа•Ва§Ь৮ а§Ха•З а§Ђа•Иа§≤ৌ৵ ১৕ৌ а§Е৮а•На§ѓ а§Еа§Ва§Ча•Ла§В а§Ха•А а§≠а§Ња§Ча•А৶ৌа§∞а•А (а§Ча•Ба§∞а•Н৶ৌ ৵ а§≤ড়৵а§∞) а§Ха•А а§Ьа§Ња§Ба§Ъ а§Ха§∞৮ৌ ু৺১а•Н৵৙а•Ва§∞а•На§£ а§єа•Иа•§
а§Ьа•З৮а•За§Яа§ња§Х ৙а§∞а•Аа§Ха•На§Ја§£ : а§ѓа§є ৙а•Ва§∞а•А ১а§∞а§є а§Єа•З а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ха•А ৙а•Ба§Ја•На§Яа§њ а§Ха§∞১ৌ а§Ьа•Л NOD2 а§Ьа•А৮ а§Ѓа•За§В а§Ца§∞а§ђа•А ৶а§∞а•Н৴ৌ১ৌ а§єа•Иа•§
 2.3 а§Ха•На§ѓа§Њ а§За§Єа§Ха§Њ а§За§≤а§Ња§Ь а§Єа§Ва§≠৵ а§єа•И а§ѓа§Њ а§За§Єа•З а§Ьа•Ь а§Єа•З а§Ѓа§ња§Яа§Ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§
2.3 а§Ха•На§ѓа§Њ а§За§Єа§Ха§Њ а§За§≤а§Ња§Ь а§Єа§Ва§≠৵ а§єа•И а§ѓа§Њ а§За§Єа•З а§Ьа•Ь а§Єа•З а§Ѓа§ња§Яа§Ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§
а§За§Єа•З ৙а•Ва§∞а•А ১а§∞а§є а§Єа•З ৆а•Аа§Х ৮৺а•Аа§В а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И а§≤а•За§Хড়৮ а§Ьа•Ла•Ьа•Ла§В, а§Жа§Ба§Ца•З ১৕ৌ а§Е৮а•На§ѓ а§Еа§Ва§Ча•Ла§В а§Ха•А а§Єа•Ва§Ь৮ а§Ха•Л а§Ха§Ња§ђа•В а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•А ৶৵ৌа§Уа§В а§Єа•З а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ ৶৵ৌа§Уа§В а§Єа•З а§≤а§Ха•На§Ја§£а•Ла§В а§Ха•Л а§Ха§Ња§ђа•В а§Ѓа•За§В а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И ১৕ৌ а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•Л а§ђа•Э৮а•З а§Єа•З а§∞а•Ла§Ха§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§
 2.4 а§За§≤а§Ња§Ь а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И ?
2.4 а§За§≤а§Ња§Ь а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И ?
৵а§∞а•Н১ুৌ৮ а§Ѓа•За§В а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ха•Ла§И а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§Ьа•Ла•Ь а§Єа§В৐৲ড়১ а§≤а§Ха•На§Ја§£а•Ла§В а§Ха•Л а§Єа•Ва§Ь৮ а§Ха§Ѓ а§Ха§∞৮а•З ৵ৌа§≤а•А ৶৵ৌа§П а§Ьа•Иа§Єа•З
৮а•Л৮ а§Єа•На§Яа•За§∞а•Йа§За§°а§≤ ৶৵ৌа§П ১৕ৌ
ুড়৕а•Ла§Яа•На§∞а•За§Ха•На§Єа•За§Я а§Єа•З ৆а•Аа§Х а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ѓа•З৕а•Ла§Яа•На§∞а•За§Ха•На§Єа•За§Я а§Ьа•Б৵а•З৮ৌа§За§≤ а§За§°а§ња§ѓа•Л৙а•З৕ড়а§Х а§Жа§∞а•Н৕а§∞а§Ња§За§Яа§ња§Є а§Ѓа•За§В а§Ч৆ড়ৃৌ а§Ха•Л а§Ха§Ња§Ђа•А ৺৶ ১а§Х а§Ха§Ња§ђа•В а§Ха§∞১ৌ а§єа•И а§≤а•За§Хড়৮ а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ѓа•За§В а§ѓа§є а§Еа§Іа§ња§Х ীৌৃ৶а•За§Ѓа§В৶ ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§ѓа•В৵ৌа§За§Яа§ња§Є а§Ха•Л а§Ха§Ња§ђа•В а§Ха§∞৮ৌ а§Х৆ড়৮ а§єа•Иа•§ а§≤а•Ла§Ха§≤ а§Єа•На§Яа•За§∞а•Ла§За§°а§≤ а§Жа§Ба§Ц а§Ха•А ৶৵ৌ а§Е৕৵ৌ а§За§Ва§Ьа•За§Ха•Н৴৮ а§Ха§И а§∞а•Ла§Ча§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•З а§≤а§ња§П ৙а§∞а•Нৃৌ৙а•Н১ ৮৺а•Аа§В а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§ а§ѓа•В৵ৌа§За§Яа§ња§Є а§Ха•З ৮ড়ৃа§В১а•На§∞а§£ а§Ѓа•За§В а§Ѓа•З৕а•Ла§Яа•На§∞а•За§Ха•На§Єа•За§Я а§єа§Ѓа•З৴ৌ ীৌৃ৶а•За§Ѓа§В৶ ৮৺а•Аа§В а§єа•Л১ৌ а§єа•И ১৕ৌ а§∞а•Ла§Ча§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•Л а§Ѓа•Ба§Ба§є а§Єа•З corticosteroids а§Ха•А а§Ж৵৴а•На§ѓа§Х১ৌ ৙а•Ь১а•А а§єа•Иа•§
а§Ха•Ба§Ы а§∞а•Ла§Ча•А а§Ьড়৮ুа•За§В а§Жа§Ба§Ца•Ла§В, а§Ьа•Ла•Ьа•Ла§В ১৕ৌ а§Ж১а§Ва§∞а§ња§Х а§Еа§Ва§Ча•Ла§В а§Ха•А а§Єа•Ва§Ь৮ а§Ха§Ња§ђа•В а§Ѓа•За§В ৮৺а•Аа§В а§єа•Л১а•А а§єа•И а§Й৮ а§∞а•Ла§Ча§ња§ѓа•Ла§В а§Ѓа•За§В cytokine - inhibitors а§Ьа•Иа§Єа•З TNF - inhibitors (
Infliximab,
Adalimumab) ৙а•На§∞а§≠ৌ৵а•А а§єа•Л১а•З а§єа•Иа•§
 2.5 а§З৮ ৶৵ৌа§Уа§В а§Ха•З а§ђа•Ба§∞а•З ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И ?
2.5 а§З৮ ৶৵ৌа§Уа§В а§Ха•З а§ђа•Ба§∞а•З ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ а§Ха•На§ѓа§Њ а§єа•И ?
а§Ѓа•З৕а•Ла§Яа•На§∞а•За§Ха•На§Єа•За§Я а§Єа•З а§єа•Л৮а•З ৵ৌа§≤а•З а§ђа•Ба§∞а•З ৙а•На§∞а§≠ৌ৵а•Ла§В а§Ѓа•За§В ুড়১а§≤а•А ১৕ৌ ৙а•За§Я а§Ѓа•За§В ৶а§∞а•Н৶ а§Єа§ђа§Єа•З а§Жа§Ѓ а§єа•Иа•§ а§Ца•В৮ а§Ха•А а§Ьа§Ња§Ба§Ъ а§≤ড়৵а§∞ а§Ха•А а§Ха§Ња§∞а•На§ѓа§Ха•Нৣু১ৌ ১৕ৌ а§Єа•Юа•З৶ а§∞а§Ха•Н১ а§Ха§£а§ња§Ха§Ња§Уа§В а§Ха•А а§Єа§Ва§Ца•На§ѓа§Њ ৶а•За§Ц৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ха•А а§Ьৌ১а•А а§єа•Иа•§ corticosteroids а§Єа•З а§єа•Л৮а•З ৵ৌа§≤а•З а§Єа§Ва§≠ৌ৵ড়১ а§ђа•Ба§∞а•З ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ ৵а§Ь৮ а§ђа•Э৮ৌ, а§Ъа•За§єа§∞а•З ৙а§∞ а§Єа•Ва§Ь৮ ১৕ৌ а§Ѓа•Ва§° а§Ѓа•За§В а§Й১ৌа§∞ а§Ъ৥ৌ৵ а§єа•Л১а•З а§єа•Иа•§ а§≤а§Ва§ђа•З а§Єа§Ѓа§ѓ ১а§Х corticosterioid а§Ха•З а§Й৙ৃа•Ла§Ч а§Єа•З а§Еа§Іа§ња§Х а§∞а§Ха•Н১ а§Ъৌ৙, а§°а§Ња§ѓа§ђа§ња§Яа•Аа§Ь, а§Ха§Ѓа§Ьа•Ла§∞ а§єа•Ьа§°а§ња§ѓа§Ња§Б ১৕ৌ ৴ৌа§∞а•Аа§∞а§ња§Х ৵ড়а§Ха§Ња§Є а§Ѓа•За§В а§∞а•Ва§Хৌ৵а§Я а§єа•Л а§Єа§Х১а•А а§єа•Иа•§
TNF-пБ° Inhibitors ৮ৃа•А ৶৵ৌа§Па§В а§єа•И - а§З৮а§Ха•З а§Й৙ৃа•Ла§Ч а§Єа•З а§З৮а•На§Ђа•За§Ха•Н৴৮ а§≤а§Ч৮а•З а§Ха§Њ а§Ц১а§∞а§Њ ১৕ৌ T. B а§єа•Л৮а•З а§Ха•А а§Єа§Ва§≠ৌ৵৮ৌ а§ђа•Э а§Єа§Х১а•А а§єа•И а§Фа§∞ ৶а•Ва§Єа§∞а•З ৮а•На§ѓа•Ва§∞а•Ла§≤а•Йа§Ьа§ња§Ха§≤ ৵ ৙а•На§∞১ড়а§∞а§Ха•На§Ја§Њ а§Єа§Ва§ђа§Ва§Іа•А а§∞а•Ла§Ча•Ла§В а§Ха•А а§Єа§Ва§≠ৌ৵৮ৌ а§ђа•Э а§Єа§Х১а•А а§єа•Иа•§ а§Ха•Иа§Ва§Єа§∞ а§Єа§Ва§ђа§Ва§Іа•А а§∞а•Ла§Ча•Ла§В а§Ха•А а§Єа§Ва§≠ৌ৵৮ৌ ৶а•За§Ца•А а§Ча§ѓа•А а§єа•И а§≤а•За§Хড়৮ а§Еа§≠а•А ১а§Х ৙а§∞а•Нৃৌ৙а•Н১ а§Ьৌ৮а§Ха§Ња§∞а•А а§Й৙а§≤а§ђа•На§І ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§
 2.6 а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ а§Хড়১৮а•З а§≤а§Ва§ђа•З а§Єа§Ѓа§ѓ ১а§Х а§Ъа§≤১ৌ а§єа•И ?
2.6 а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ а§Хড়১৮а•З а§≤а§Ва§ђа•З а§Єа§Ѓа§ѓ ১а§Х а§Ъа§≤১ৌ а§єа•И ?
а§Еа§≠а•А ১а§Х а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ а§Ха§Њ а§Еа§Іа§ња§Х১ু а§Єа§Ѓа§ѓ ৮ড়а§∞а•На§Іа§Ња§∞ড়১ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ха•Ла§И а§Ьৌ৮а§Ха§Ња§∞а•А а§Й৙а§≤а§ђа•На§І ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§Ьа•Ла•Ь, а§Жа§Ба§Ц ১৕ৌ а§Е৮а•На§ѓ а§Еа§Ва§Ча•Л а§Ха•А а§Ца§∞а§Ња§ђа•А а§∞а•Ла§Х৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Єа•Ва§Ь৮ а§Ха•Л а§Ха§Ња§ђа•В а§Ха§∞৮ৌ а§Ж৵৴а•На§ѓа§Х а§єа•Иа•§
 2.7 а§Ха•На§ѓа§Њ а§Е৙а§∞а§В৙а§∞а§Ња§Ч১ а§ѓа§Њ ৙а•Ва§∞а§Х а§Ъа§ња§Хড়১а•На§Єа§Њ а§Ха§Њ а§Ха•Ла§И а§Й৙ৃа•Ла§Ч а§єа•Иа•§
2.7 а§Ха•На§ѓа§Њ а§Е৙а§∞а§В৙а§∞а§Ња§Ч১ а§ѓа§Њ ৙а•Ва§∞а§Х а§Ъа§ња§Хড়১а•На§Єа§Њ а§Ха§Њ а§Ха•Ла§И а§Й৙ৃа•Ла§Ч а§єа•Иа•§
а§За§Є ১а§∞а§є а§Ха•А а§Ъа§ња§Хড়১а•На§Єа§Њ а§Ха•А а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ѓа•За§В а§Ха•Ла§И а§Й৙ৃа•Ла§Чড়১ৌ ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§
 2.8 а§Єа§Ѓа§ѓ а§Єа§Ѓа§ѓ ৙а§∞ а§Хড়৮ а§Ьа§Ња§Ва§Ъа•Л а§Ха§Њ а§єа•Л৮ৌ а§Ьа§∞а•Ба§∞а•А а§єа•И?
2.8 а§Єа§Ѓа§ѓ а§Єа§Ѓа§ѓ ৙а§∞ а§Хড়৮ а§Ьа§Ња§Ва§Ъа•Л а§Ха§Њ а§єа•Л৮ৌ а§Ьа§∞а•Ба§∞а•А а§єа•И?
а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•А ৮ড়ৃুড়১ а§∞а•В৙ а§Єа•З ৙а•Аа§°а§ња§ѓа§Ња§Яа•На§∞а§ња§Х Rheumatologist ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ а§Ьа§Ња§Ба§Ъ (а§Ха§Ѓ а§Єа•З а§Ха§Ѓ а§Єа§Ња§≤ а§Ѓа•За§В а•© а§ђа§Ња§∞) а§єа•Л৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§П а§Ьа§ња§Єа§Єа•З а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха§Њ ৮ড়ৃа§В১а•На§∞а§£ ১৕ৌ а§Ѓа•За§°а§ња§Ха§≤ а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ ৆а•Аа§Х ১а§∞а§є а§Єа•З а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И а•§а§Жа§Ба§Ца•Ла§В а§Ха•З ৵ড়৴а•За§Ја§Ьа•На§Ю а§Ха§Њ ৙а§∞а§Ња§Ѓа§∞а•Н৴ ৮ড়ৃুড়১ а§∞а•В৙ а§Єа•З а§≤а•З৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§ а§Ьа•Л а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ а§Ха•З а§Еа§В১а§∞а•На§Ч১ а§єа•Иа§В а§Й৮а§Ха§Њ а§Ха§Ѓ а§Єа•З а§Ха§Ѓ ৵а§∞а•На§Ј а§Ѓа•За§В ৶а•Л а§ђа§Ња§∞ а§Ца•В৮ ১৕ৌ ৙а•З৴ৌ৐ а§Ха•А а§Ьа§Ња§Ба§Ъ а§єа•Л৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§
 2.9 а§ѓа§є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Хড়১৮а•З а§≤а§Ва§ђа•З а§Єа§Ѓа§ѓ ১а§Х а§∞৺১а•А а§єа•И?
2.9 а§ѓа§є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Хড়১৮а•З а§≤а§Ва§ђа•З а§Єа§Ѓа§ѓ ১а§Х а§∞৺১а•А а§єа•И?
а§ѓа§є а§Ьа•А৵৮ а§≠а§∞ а§∞৺৮а•З৵ৌа§≤а•А а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•И а§≤а•За§Хড়৮ а§Єа§Ѓа§ѓ а§Ха•З ৪ৌ৕ а§Ха§Ѓ а§Ьа•Нৃৌ৶ৌ а§єа•Л а§Єа§Х১а•А а§єа•Иа•§
 2.10 а§≤а§Ва§ђа•А а§Е৵৲ড় а§Ѓа•За§В а§За§Є а§∞а•Ла§Ч а§Ха§Њ а§≠৵ড়ৣа•На§ѓ а§Ѓа•За§В а§Ха•На§ѓа§Њ ৙а§∞а§ња§£а§Ња§Ѓ ৵ а§Ха•Ла§∞а•На§Є а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•И?
2.10 а§≤а§Ва§ђа•А а§Е৵৲ড় а§Ѓа•За§В а§За§Є а§∞а•Ла§Ч а§Ха§Њ а§≠৵ড়ৣа•На§ѓ а§Ѓа•За§В а§Ха•На§ѓа§Њ ৙а§∞а§ња§£а§Ња§Ѓ ৵ а§Ха•Ла§∞а•На§Є а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•И?
а§≤а§Ва§ђа•А а§Е৵৲ড় а§Ѓа•За§В а§За§Є а§∞а•Ла§Ч а§Ха•З ৮ড়৶ৌ৮ а§Ха•А а§Ьৌ৮а§Ха§Ња§∞а•А а§Єа•Аুড়১ а§єа•Иа•§ а§Ха•Ба§Ы а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•Л а•®а•¶ ৵а§∞а•На§Ја•Ла§В ১а§Х ৮ড়а§Ча§∞ৌ৮а•А а§Ѓа•За§В а§∞а§Ца§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•И а§Фа§∞ а§Й৮а§Ха§Њ ৴ৌа§∞а•Аа§∞а§ња§Х ৵ ুৌ৮৪ড়а§Х ৵ড়а§Ха§Ња§Є ৪ৌুৌ৮а•На§ѓ а§єа•Л১ৌ а§єа•И ১৕ৌ а§Еа§Ъа•На§Ыа•З а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ а§Єа•З ৪ৌুৌ৮а•На§ѓ а§Ьа•А৵৮ ৃৌ৙৮ а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§Ва•§
 2.11 а§Ха•На§ѓа§Њ ৙а•Ва§∞а•А ১а§∞а§є а§Єа•З ৆а•Аа§Х а§єа•Л৮ৌ а§Єа§Ва§≠৵ а§єа•И?
2.11 а§Ха•На§ѓа§Њ ৙а•Ва§∞а•А ১а§∞а§є а§Єа•З ৆а•Аа§Х а§єа•Л৮ৌ а§Єа§Ва§≠৵ а§єа•И?
৮৺а•Аа§В, а§Ха•На§ѓа•Ла§Ва§Ха§њ а§ѓа§є а§Па§Х а§Ж৮а•Б৵а§В৴ড়а§Х а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§єа•Иа•§ а§Ђа§ња§∞ а§≠а•А а§Па§Х а§Еа§Ъа•На§Ыа•А а§°а•Йа§Ха•На§Яа§∞а•А а§Ьа§Ња§Ба§Ъ ১৕ৌ а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ а§Єа•З а§Па§Х а§Еа§Ъа•На§Ыа§Њ а§Ьа•А৵৮ ৃৌ৙৮ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ха•З а§Ѓа§∞а•Аа§Ьа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха§Њ ৵ড়а§Ха§Ња§Є ১৕ৌ ১а•А৵а•На§∞১ৌ а§Еа§≤а§Ч а§Еа§≤а§Ч а§єа•Л১а•А а§єа•И, ৵а§∞а•Н১ুৌ৮ а§Ѓа•За§В ৙а•На§∞১а•На§ѓа•За§Х а§∞а•Ла§Ча•А а§Ѓа•За§В а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха§Њ а§Ха•Ла§∞а•На§Є ৮ড়а§∞а•На§Іа§Ња§∞ড়১ а§Ха§∞৮ৌ а§Єа§Ва§≠৵ ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§
 3.1 а§ѓа§є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§∞а•Ла§Ча•А а§Фа§∞ а§Йа§Єа§Ха•З ৙а§∞ড়৵ৌа§∞ ৙а§∞ а§Ха•На§ѓа§Њ а§Еа§Єа§∞ а§Ха§∞১а•А а§єа•И ?
3.1 а§ѓа§є а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§∞а•Ла§Ча•А а§Фа§∞ а§Йа§Єа§Ха•З ৙а§∞ড়৵ৌа§∞ ৙а§∞ а§Ха•На§ѓа§Њ а§Еа§Єа§∞ а§Ха§∞১а•А а§єа•И ?
а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•З ৮ড়৶ৌ৮ а§Ха•З ৙а•Ва§∞а•Н৵ а§Ха§И а§Єа§Ѓа§Єа•На§ѓа§Ња§Уа§Ва§Ха§Њ а§Ха§Њ ৪ৌু৮ৌ а§Ха§∞৮ৌ ৙а•Ь১ৌ а§єа•Иа•§ а§Па§Х а§ђа§Ња§∞ а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•А ৙а•Ба§Ја•На§Яа§њ а§єа•Л৮а•З ৙а§∞ а§∞а•Ла§Ча•А а§Ха•Л ৮ড়ৃুড়১ а§∞а•В৙ а§Єа•З а§Ъа§ња§Хড়১а•На§Єа§Х (৙а•Аа§°а§ња§ѓа§Ња§Яа•На§∞а§ња§Х Rheumatologist ১৕ৌ ৮а•З১а•На§∞ а§∞а•Ла§Ч ৵ড়৴а•За§Ја§Ьа•На§Ю) а§Ха§Њ ৙а§∞а§Ња§Ѓа§∞а•Н৴ а§≤а•З৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§П а§Ьа§ња§Єа§Єа•З а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•А а§Єа§Ха•На§∞ড়ৃ১ৌ а§Ха•Л ুৌ৙ৌ а§Ьа§Њ а§Єа§Ха•З ১৕ৌ а§Й৙а§Ъа§Ња§∞ а§Ха•Л а§Єа§Ѓа§Ња§ѓа•Ла§Ьড়১ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Ха•За•§ а§Ьа•Ла•Ьа•Ла§В а§Ха•А а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ѓа•За§В а§Ђа§ња§Ьа§ња§ѓа•Л৕а•За§∞а•З৙а•А а§Ха•А а§Ж৵৴а•На§ѓа§Х১ৌ а§єа•Л১а•А а§єа•Иа•§
 3.2 а§Ха•На§ѓа§Њ а§ђа§Ъа•На§Ъа§Њ а§Єа•На§Ха•Ва§≤ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И?
3.2 а§Ха•На§ѓа§Њ а§ђа§Ъа•На§Ъа§Њ а§Єа•На§Ха•Ва§≤ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И?
а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•З а§≤а§Ва§ђа•З а§Ха•Ла§∞а•На§Є а§Ха•А ৵а§Ьа§є а§Єа•З а§ђа§Ъа•На§Ъа•За§В а§Ха•А а§Єа•На§Ха•Ва§≤ а§Ѓа•За§В ৮ড়ৃুড়১১ৌ ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ড়১ а§єа•Л а§Єа§Х১а•А а§єа•Иа•§ а§Єа•На§Ха•Ва§≤ а§Ѓа•За§В а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•А ৙а•Ва§∞а•А а§Ьৌ৮а§Ха§Ња§∞а•А а§єа•Л৮а•А а§Ъа§Ња§єа§ња§П а§Ьа§ња§Єа§Єа•З а§За§Єа§Ха•З а§≤а§Ха•На§Ја§£ а§Ж৮а•З ৙а§∞ а§Ха•На§ѓа§Њ а§Фа§∞ а§Ха•Иа§Єа•З а§Ха§∞৮ৌ а§єа•И а§За§Єа§Ха•А а§Єа§≤а§Ња§є ৶а•А а§Ьа§Њ а§Єа§Х১а•А а§єа•Иа•§
 3.3 а§Ха•На§ѓа§Њ а§Ца•За§≤а§Ха•В৶ а§Ѓа•За§В а§≠а§Ња§Ч а§≤а•З а§Єа§Х১а•З а§єа•И ?
3.3 а§Ха•На§ѓа§Њ а§Ца•За§≤а§Ха•В৶ а§Ѓа•За§В а§≠а§Ња§Ч а§≤а•З а§Єа§Х১а•З а§єа•И ?
а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ха•З а§ђа§Ъа•На§Ъа•Ла§В а§Ха•Л а§Ца•За§≤а§Ха•В৶ а§Ха•З а§≤а§ња§П ৙а•На§∞а•За§∞ড়১ а§Ха§∞৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§П, ৙а§∞ а§Ха•На§ѓа§Њ а§Фа§∞ а§Хড়১৮ৌ ৮ড়а§∞а•На§≠а§∞ а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§
 3.4 а§≠а•Ла§Ь৮ а§Ха•Иа§Єа§Њ а§єа•Л৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§П?
3.4 а§≠а•Ла§Ь৮ а§Ха•Иа§Єа§Њ а§єа•Л৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§П?
а§Ха•Ла§И ৵ড়৴ড়ৣа•На§Я а§≠а•Ла§Ь৮ ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ ৃ৶ড় а§ђа§Ъа•На§Ъа§Њ corticosteroids ৶৵ৌа§Уа§В ৙а§∞ а§єа•Иа§В ১৐ а§Е১ড়а§∞а§ња§Ха•Н১ а§Ѓа•А৆ৌ а§Фа§∞ ৮ুа§Ха•А৮ ৵а§∞а•На§Ьড়১ а§єа•Иа•§
 3.5 а§Ха•На§ѓа§Њ а§Ѓа•Ма§Єа§Ѓ а§Ха§Њ а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•З а§Ха•Ла§∞а•На§Є ৙а§∞ а§Ха•Ла§И ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ ৙а•Ь১ৌ а§єа•И?
3.5 а§Ха•На§ѓа§Њ а§Ѓа•Ма§Єа§Ѓ а§Ха§Њ а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•З а§Ха•Ла§∞а•На§Є ৙а§∞ а§Ха•Ла§И ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ ৙а•Ь১ৌ а§єа•И?
৮৺а•Аа§Ва•§
 3.6 а§Ха•На§ѓа§Њ а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ха§Њ а§Яа•Аа§Ха§Ња§Ха§∞а§£ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И ?
3.6 а§Ха•На§ѓа§Њ а§ђа§Ъа•На§Ъа•З а§Ха§Њ а§Яа•Аа§Ха§Ња§Ха§∞а§£ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И ?
а§Яа•Аа§Ха§Ња§Ха§∞а§£ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Њ а§Єа§Х১ৌ а§єа•И а§≤а•За§Хড়৮ а§Ьа•Л а§∞а•Ла§Ча•А corticosteroid, а§Ѓа•З৕а•Ла§Яа•На§∞а•За§Ха•На§Єа•За§Я ৵ TNF Inhibitors ৙а§∞ а§єа•Иа§В а§Й৮ а§Ха•Л а§Ьа•И৵ড়а§Х а§Яа§ња§Ха•З ৮৺а•Аа§В ৶а•З৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§
 3.7 а§ѓа•М৮ а§Ьа•А৵৮, а§Ча§∞а•На§≠ৌ৵৪а•Н৕ৌ ১৕ৌ а§Ь৮а•На§Ѓ ৮ড়ৃа§В১а•На§∞а§£ ৙а§∞ ৙а•На§∞а§≠ৌ৵?
3.7 а§ѓа•М৮ а§Ьа•А৵৮, а§Ча§∞а•На§≠ৌ৵৪а•Н৕ৌ ১৕ৌ а§Ь৮а•На§Ѓ ৮ড়ৃа§В১а•На§∞а§£ ৙а§∞ ৙а•На§∞а§≠ৌ৵?
а§ђа•На§≤а§Ња§Й а§Єа§ња§Ва§°а•На§∞а•Ла§Ѓ а§Ха•З а§Ѓа§∞а•Аа§Ьа•Ла§В а§Ѓа•За§В а§ђа•Аа§Ѓа§Ња§∞а•А а§Ха•А ৵а§Ьа§є а§Єа•З ৙а•На§∞а§Ь৮৮ а§Ха•А а§Єа§Ѓа§Єа•На§ѓа§Њ ৮৺а•Аа§В а§єа•Л১а•А а§єа•Иа•§ ৃ৶ড় ৵а•З а§Ѓа•И৕а•Ла§Яа•На§∞а•За§Ха•На§Єа•За§Я ৙а§∞ а§єа•И ১а•Л а§Ь৮а•На§Ѓ ৮ড়ৃа§В১а•На§∞а§£ а§Ха§∞৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§П а§Ха•На§ѓа•Ла§Ва§Ха§њ а§ѓа§є ৶৵ৌ а§≠а•На§∞а•Ва§£ ৙а§∞ ৶а•Ба§Ја•Н৙а•На§∞а§≠ৌ৵ а§°а§Ња§≤১а•А а§єа•Иа•§ TNF Inhibitors ১৕ৌ а§Ча§∞а•На§≠৵৪а•Н৕ৌ а§Ха•З а§ђа§Ња§∞а•З а§Ѓа•За§В а§Ха•Ла§И а§Єа•Ба§∞а§Ха•На§Ја§Њ а§Єа§В৐৲ড়১ а§Ьৌ৮а§Ха§Ња§∞а•А а§Й৙а§≤а§ђа•На§І ৮৺а•Аа§В а§єа•И а§За§Єа§≤а§ња§П а§Ча§∞а•На§≠ а§Іа§Ња§∞а§£ а§Ха§∞৮а•З а§Єа•З ৙৺а§≤а•З а§З৮ ৶৵ৌа§Уа§В а§Ха•Л а§ђа§В৶ а§Ха§∞ ৶а•З৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§